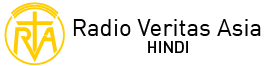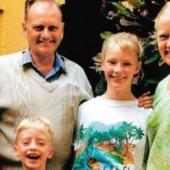दलित ईसाई संवैधानिक समानता और आध्यात्मिक समावेश के हकदार हैं

तमिलनाडु के गांवों और भारत के शहरी इलाकों में, हर दिन एक गहरा विरोधाभास सामने आता है।
ग्रामीण तमिलनाडु की दलित ईसाई मरियम्माल कहती हैं, "मेरा विश्वास सिखाता है कि ईश्वर के सामने सभी समान हैं, फिर भी मैं अपने इलाके के अन्य लोगों की तरह एक ही भोज के प्याले से नहीं पी सकती।"
उनका अनुभव भारत के लाखों पूर्व "अछूतों" के सामने आने वाले दर्दनाक विरोधाभास का उदाहरण है, जिन्होंने सम्मान की तलाश में ईसाई धर्म अपना लिया, लेकिन वे खुद को दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ पाते हैं।
सदियों से, भारत की कठोर जाति व्यवस्था ने दलितों को समाज के हाशिये पर धकेल दिया, उन्हें बुनियादी अधिकारों और अवसरों से वंचित किया जबकि उन पर "अशुद्धता" थोपी जो उनके अलगाव को उचित ठहराती थी।
जब ईसाई धर्म आया, मसीह में समानता का वादा करते हुए, कई लोगों ने मुक्ति के मार्ग के रूप में धर्मांतरण को अपनाया। फिर भी औपनिवेशिक शासन और स्वदेशी सत्ता संरचनाओं ने यह सुनिश्चित किया कि जाति पदानुक्रम ईसाई समुदायों में घुसपैठ करे, जिससे चर्च की दीवारों के भीतर भेदभाव की समानांतर व्यवस्था बन गई।
स्वतंत्रता के बाद, भारत के संविधान ने अस्पृश्यता को गैरकानूनी घोषित कर दिया और ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की स्थापना की।
हालांकि, 1950 के संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश ने इन सुरक्षाओं को हिंदू दलितों तक सीमित करके, बाद में उन्हें सिखों और बौद्धों तक बढ़ाकर, लेकिन ईसाइयों और मुसलमानों को बाहर रखकर एक अभूतपूर्व दुविधा पैदा कर दी।
यह नीति एक अविवेकी विकल्प को मजबूर करती है: शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुँचने के लिए आधिकारिक तौर पर हिंदू पहचान बनाए रखें, या खुले तौर पर ईसाई धर्म को अपनाएँ और संवैधानिक सुरक्षा को त्याग दें।
जैसा कि डॉ. सुखदेव थोरात के शोध से लगातार पता चलता है, धर्म परिवर्तन दैनिक जीवन में जाति के कलंक को मिटा नहीं सकता।
वे तर्क देते हैं, "धार्मिक संबद्धता के आधार पर मानवीय गरिमा को विभाजित नहीं किया जा सकता है।" "जब राज्य सामाजिक न्याय को धार्मिक पहचान से जोड़ता है, तो यह धर्मनिरपेक्षता और समानता दोनों को कमजोर करता है।"
यह विरोधाभास भारत के संवैधानिक वादे के मूल में है। दूरदर्शी प्रस्तावना सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की गारंटी देती है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है, अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकता है, और अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
फिर भी 1950 का आदेश एक ऐसी व्यवस्था बनाता है जहाँ भेदभाव के समान अनुभवों को राज्य से केवल धार्मिक संबद्धता के आधार पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ मिलती हैं।
तमिलनाडु में कोट्टापलायम पैरिश की अपील पर सुनवाई करने का सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय एक संभावित मोड़ है, जो पहली बार इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि क्या संवैधानिक सुरक्षा धार्मिक स्थानों तक विस्तारित होती है जब मौलिक मानवीय गरिमा दांव पर होती है।
यह संघर्ष कानूनी श्रेणियों से परे है, मौलिक मानवीय गरिमा की बात करता है - जन्म, विश्वास या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना हर व्यक्ति का अंतर्निहित मूल्य।
चेन्नई के एक दलित ईसाई कार्यकर्ता थॉमस राजा इस वास्तविकता को स्पष्ट करते हैं: "जब मुझे बताया जाता है कि मेरे चढ़ावे से चर्च के समारोह 'दूषित' होंगे, तो यह न केवल मेरे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है- यह मेरी मानवता से वंचित होना है। पूरी तरह से मानव होने का मतलब है सामुदायिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेना।"
यह बहिष्कार कई तरीकों से प्रकट होता है: पवित्र मिस्सा में अलग बैठने की व्यवस्था, पैरिश काउंसिल से बहिष्कार, नेतृत्व की भूमिकाओं से अस्वीकृति, और अलग कब्रिस्तान। प्रत्येक अभ्यास एक ही विनाशकारी संदेश देता है: भगवान के कुछ बच्चों को दूसरों की तुलना में कम योग्य माना जाता है।
जबकि कानूनी लड़ाई जारी है, कैथोलिक चर्च में सामाजिक परिवर्तन की जबरदस्त क्षमता है।
कैथोलिक धर्मशास्त्री वर्जीनिया सालदान्हा का सुझाव है, "इस संघर्ष में चर्च सबसे शक्तिशाली परिवर्तन एजेंट हो सकता है।" "जब सेंट पॉल ने घोषणा की कि 'न तो यहूदी है और न ही यूनानी, न ही गुलाम और न ही स्वतंत्र,' उन्होंने समानता को एक गैर-परक्राम्य ईसाई मूल्य के रूप में स्थापित किया। चर्च को इस क्रांतिकारी दृष्टि को पुनः प्राप्त करना चाहिए।"
प्रगतिशील सूबाओं ने प्रदर्शित किया है कि जानबूझकर की गई कार्रवाई के माध्यम से परिवर्तन संभव है, जिसमें समावेशी धार्मिक प्रथाएं, नेतृत्व के पदों पर दलित ईसाइयों के लिए प्रतिनिधित्व की गारंटी, चर्च की संपत्तियों का एकीकरण और ऐतिहासिक नुकसानों को संबोधित करने वाले आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम शामिल हैं।
अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्गों के लिए CBCI कार्यालय के पूर्व सचिव फादर देवसागयाराज बताते हैं, "ये रियायतें नहीं बल्कि सुधार हैं।" "वे चर्च की प्रथाओं को चर्च की शिक्षा के साथ जोड़ते हैं।"
परिवर्तन रातों-रात नहीं हो सकता। सदियों से जड़े पूर्वाग्रहों को खत्म करने के लिए धैर्य और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। आगे का रास्ता तात्कालिक प्रतीकात्मक कार्रवाइयों को दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तनों के साथ जोड़ता है।
तात्कालिक कदमों में अतीत के भेदभाव को औपचारिक रूप से स्वीकार करना, कब्रिस्तानों सहित अलग-अलग सुविधाओं को एकीकृत करना और धार्मिक सेवाओं में समान भागीदारी शामिल है।
मध्यम अवधि के परिवर्तनों में व्यापक शिक्षा कार्यक्रम शामिल हैं जो जातिगत पूर्वाग्रह को संबोधित करते हैं, प्रतिनिधित्व कोटा जो सुनिश्चित करते हैं कि दलित ईसाई नेतृत्व की स्थिति में हों, और आर्थिक सशक्तिकरण पहल।