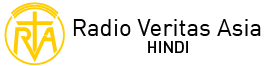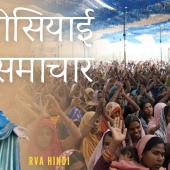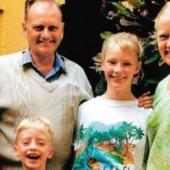भारत-पाकिस्तान संबंध खतरनाक मोड़ पर हैं

कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में पर्यटकों पर हुए विनाशकारी आतंकवादी हमले ने भारत और पाकिस्तान को खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है।
पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा की शाखा रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) के चार आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक सहित 26 पर्यटक मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। टीआरएफ ने औपचारिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए इस क्षेत्र में गैर-कश्मीरियों के बसने के विरोध को अपना मकसद बताया।
मृतकों में एक ईसाई और एक मुस्लिम टट्टू चालक शामिल हैं, जबकि बाकी भारत के विभिन्न हिस्सों से आए हिंदू पुरुष हैं।
हत्यारों द्वारा हिंदू पुरुषों को निशाना बनाए जाने और महिलाओं तथा मुस्लिम पर्यटक अनुरक्षकों और सहायकों को बख्श दिए जाने के आरोपों के बीच मृतकों का धर्म तुरंत महत्वपूर्ण हो गया, जिसने सोशल मीडिया पर एक जहरीले और सांप्रदायिक रूप से आवेशित इस्लामोफोबिक प्रवचन को बढ़ावा दिया।
भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु शस्त्रागार है, और दोनों देशों में हो रहे घटनाक्रमों पर गहरी चिंता के साथ नज़र रखी जा रही है।
देशों के बीच फिर से भड़के तनाव में, भारत ने बहुत ही कठोर उपायों की घोषणा की, जिसमें पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमा को बंद करना, अपने सैन्य पर्यवेक्षकों को अवांछित घोषित करना, उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या में कटौती करना और सबसे असामान्य रूप से, अरब सागर में जाने के रास्ते में पश्चिमी पंजाब में बहने वाली विशाल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल को साझा करने की सात दशक पुरानी संधि को निलंबित करना शामिल है।
भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करना एक महत्वपूर्ण वृद्धि के रूप में देखा जा रहा है। सिंधु नदी प्रणाली पर अत्यधिक निर्भर पाकिस्तान को गंभीर आर्थिक और कृषि चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है यदि संधि का निलंबन जारी रहता है, जिससे संभावित रूप से जवाबी कार्रवाई हो सकती है।
सिंधु जल-बंटवारा संधि 1947 में विभाजन के बाद से भारत के चार औपचारिक युद्धों से बची हुई है।
तिब्बती पठार में उगने वाली सिंधु नदी पाकिस्तान की जीवन रेखा है, और इसके जल को भारत द्वारा अपने क्षेत्र में नदी के बहुत छोटे हिस्से के साथ बनाए गए हेडवर्क्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
पहलगाम हमले ने उस क्षेत्र में पर्यटकों को निशाना बनाया, जिसने हाल के वर्षों में अपेक्षाकृत शांति के कारण पर्यटन में उछाल देखा है। नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाना, कश्मीर के हाल के इतिहास में एक दुर्लभ घटना, स्थिरता के भ्रम को चकनाचूर कर देती है।
इसलिए, यह हमला हाल के वर्षों में जम्मू और कश्मीर में हासिल की गई आर्थिक और सामाजिक प्रगति को खतरे में डालता है। इस क्षेत्र में पर्यटन में उछाल देखा गया है, 2024 में 3.5 मिलियन आगंतुकों के साथ, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हमले ने पर्यटकों के तत्काल पलायन को प्रेरित किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हमले के समय सऊदी अरब में थे - संयोग से अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने परिवार के साथ तीन दिवसीय यात्रा पर थे - ने अपराधियों को "दुनिया के कोने-कोने तक" खदेड़ने की कसम खाई। उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों को भी हाई अलर्ट पर रखा है। फ्रांस और अमेरिका से खरीदे गए युद्धक विमानों और इजरायल से प्राप्त उच्च प्रौद्योगिकी उपकरणों के साथ सशस्त्र बल अपनी सबसे मजबूत स्थिति में हैं।
इस दशक की शुरुआत में हुई झड़प के बाद भारत और चीन के बीच उत्तरी क्षेत्र में संबंध भी सुधर रहे हैं, जिससे भारत को पाकिस्तान के साथ अपने पश्चिमी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना पड़ रहा है।
पाकिस्तान की प्रतिक्रिया नपी-तुली रही है, लेकिन भारतीय गुस्से को शांत करने के लिए अपर्याप्त है। पाकिस्तान ने इसमें शामिल होने से इनकार किया, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आरोपों को भारत के भीतर "घरेलू" मुद्दे बताकर खारिज कर दिया।
पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने जानमाल के नुकसान पर संवेदना और चिंता व्यक्त की, लेकिन इस क्षेत्र को "भारतीय अवैध रूप से कब्जे वाला जम्मू और कश्मीर" कहा, जिससे तनाव और बढ़ गया।
भारत और पाकिस्तान, जो क्रमशः 1974 और 1998 से परमाणु शक्ति संपन्न हैं, का इतिहास तीन पूर्ण पैमाने के युद्धों (1947, 1965, 1971) और कारगिल (1999) में सीमित संघर्ष से भरा हुआ है, जो मुख्य रूप से कश्मीर को लेकर था।
सियाचिन ग्लेशियर, जिसे अक्सर "दुनिया का सबसे ऊंचा युद्धक्षेत्र" कहा जाता है, 1980 के दशक से ही विवाद का विषय रहा है, जहां दोनों देशों ने इस दुर्गम क्षेत्र में महंगी सैन्य उपस्थिति बनाए रखी है। नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर लगातार झड़पों के बावजूद, दोनों देशों ने सियाचिन के बाद से पूर्ण पैमाने पर सैन्य अभियानों में वृद्धि से बचने के लिए संयम बरता है।
यह संयम उनकी परमाणु क्षमताओं की पारस्परिक मान्यता से उपजा है, जो किसी भी संघर्ष के दांव को बढ़ाता है। 1972 के शिमला समझौते ने एलओसी की स्थापना की, और 1988 के परमाणु गैर-हमला प्रतिज्ञा जैसे विश्वास-निर्माण उपायों ने परमाणु वृद्धि को रोकने में मदद की है।
पिछले संकटों, जैसे 2001 में भारतीय संसद पर हमला और 2008 में मुंबई हमले, ने दोनों देशों को संघर्ष के करीब ला दिया था, लेकिन कूटनीतिक हस्तक्षेप और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण युद्ध टल गया।