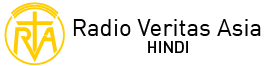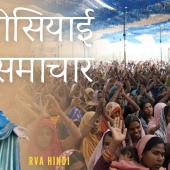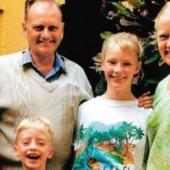भारत का असमान शैक्षिक परिदृश्य

तमिलनाडु दशकों से भारत की तीन-भाषा नीति का दृढ़ता से विरोध करता रहा है, प्रांतीय हठ के कारण नहीं बल्कि मौलिक रूप से असमान व्यवस्था के विरुद्ध एक सैद्धांतिक रुख के कारण।
दक्षिणी राज्य द्वारा अपने विद्यालयों में मूल तमिल और अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा को लागू करने के संघीय सरकार के दबाव को अस्वीकार करने की गहरी ऐतिहासिक जड़ें और सम्मोहक शैक्षिक औचित्य हैं।
यह प्रतिरोध स्वतंत्रता-पूर्व भारत में तब शुरू हुआ जब 1930 के दशक में मद्रास प्रेसीडेंसी के विद्यालयों में हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया, जिसके कारण द्रविड़ नेता पेरियार ई.वी. रामासामी के नेतृत्व में उग्र विरोध प्रदर्शन हुए।
यह पैटर्न 1965 के विस्फोटक हिंदी विरोधी आंदोलन के साथ जारी रहा, जो तब भड़क उठा जब संघीय सरकार ने हिंदी को भारत की एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने का प्रयास किया। इन विरोधों ने नई दिल्ली को अंग्रेजी को अनिश्चित काल तक सह-आधिकारिक भाषा के रूप में बनाए रखने के लिए मजबूर किया।
इसके मूल में, यह मुद्दा केवल प्रशासनिक नीति से परे है। तमिल केवल एक क्षेत्रीय बोली नहीं है - यह दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में से एक है जिसकी साहित्यिक परंपरा दो सहस्राब्दियों से भी अधिक पुरानी है।
तमिल लोगों के लिए, उनकी भाषा उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। जैसा कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि ने एक बार कहा था, "जो लोग हिंदी थोपने की वकालत करते हैं, वे कभी नहीं समझ पाए कि एक भाषा में सभ्यता की आत्मा होती है।"
भारत सरकार के तीन-भाषा फॉर्मूले के खिलाफ सबसे सम्मोहक तर्क इसका असमान कार्यान्वयन है।
उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे हिंदी भाषी उत्तरी राज्यों में, छात्र प्रभावी रूप से केवल दो भाषाएँ सीखते हैं: हिंदी (उनकी मातृभाषा) और अंग्रेजी। किसी भी तीसरी भाषा की आवश्यकता को आमतौर पर औपचारिकता के रूप में माना जाता है - खराब तरीके से पढ़ाया जाता है और जल्दी ही भूल जाता है।
ये क्षेत्र कार्यात्मक रूप से हिंदी के आधार पर एक-भाषा प्रणाली के रूप में काम करते हैं।
इस बीच, तमिलनाडु के बच्चों को वास्तव में तीन-भाषाई बोझ का सामना करना पड़ेगा: तमिल में महारत हासिल करना, अंग्रेजी में दक्षता हासिल करना (वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक), और फिर हिंदी के साथ संघर्ष करना - एक ऐसी भाषा जिसका उनके दैनिक जीवन या राज्य के भीतर भविष्य के करियर में सीमित व्यावहारिक मूल्य है।
यह असमानता दक्षिण भारतीय छात्रों के लिए एक शैक्षणिक दंड का कारण बनती है, जिन्हें अपना कीमती समय तीसरी भाषा सीखने में लगाना पड़ता है, जबकि उनके उत्तरी समकक्ष मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
कोयंबटूर में एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका मार्गरेट इस असमानता को प्रत्यक्ष रूप से देखती हैं: "हमारे छात्र पहले से ही एक अतिभारित पाठ्यक्रम से जूझ रहे हैं। जब हमने एक हिंदी पायलट कार्यक्रम शुरू किया, तो इन बच्चों ने एक ऐसी भाषा सीखने में घंटों बिताए, जिसका वे अपने समुदाय में कभी उपयोग नहीं करेंगे, जबकि वे अपने भविष्य के लिए महत्वपूर्ण विषयों में पिछड़ गए। इस बीच, उत्तरी राज्यों के स्कूल अपनी नाममात्र की 'तीसरी भाषा' कक्षाओं को मुश्किल से छूते हैं। अन्याय स्पष्ट है।"
तमिलनाडु में एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) की नेता, सांसद कनिमोझी करुणानिधि, मूल प्रश्न को स्पष्ट करती हैं: "जब दिल्ली में एक बच्चे को तमिल सीखने की आवश्यकता नहीं है, तो चेन्नई में एक बच्चे को हिंदी क्यों सीखनी चाहिए? यह राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में नहीं है - यह सांस्कृतिक वर्चस्व के बारे में है।"
तीन-भाषा नीति के समर्थकों का तर्क है कि हिंदी का ज्ञान तमिल छात्रों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाता है। फिर भी यह दावा जांच के दौरान दम तोड़ देता है।
चेन्नई और बेंगलुरु में तकनीकी कंपनियाँ मुख्य रूप से अंग्रेज़ी में कारोबार करती हैं। स्थानीय उद्योग तमिल में काम करते हैं। हिंदी प्रवीणता का कथित आर्थिक लाभ तमिलनाडु के अधिकांश निवासियों के लिए सैद्धांतिक बना हुआ है - एक दूरगामी लाभ जो तत्काल शैक्षिक लागतों को उचित नहीं ठहराता है।
तमिलनाडु तमिल और अंग्रेज़ी की अपनी दो-भाषा नीति के तहत दशकों से फल-फूल रहा है। इस संतुलित दृष्टिकोण ने स्नातकों की पीढ़ियों को तैयार किया है जो तीसरी भाषा की आवश्यकता के बिना विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं।
राज्य साक्षरता, उच्च शिक्षा नामांकन और आर्थिक विकास में लगातार उच्च स्थान पर है। हिंदी को जोड़ने से इस सफल शैक्षिक मॉडल में बाधा आएगी और कोई स्पष्ट शैक्षणिक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
जबकि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाषा विकल्पों में लचीलापन प्रदान करने का दावा करती है, यह स्पष्ट स्वतंत्रता खोखली लगती है जब हिंदी को अनुपातहीन धन और संस्थागत समर्थन मिलता है।
2019 में, हिंदी को विकास के लिए 500 मिलियन रुपये (US$5.8 मिलियन) मिले जबकि अन्य अनुसूचित भाषाओं को कुछ भी नहीं मिला - नीति की वास्तविक प्राथमिकताओं को उजागर करता है।
यह विवाद संघवाद पर एक महत्वपूर्ण लड़ाई का भी प्रतिनिधित्व करता है। शिक्षा मूल रूप से भारत के संविधान के तहत एक राज्य का विषय था, जो क्षेत्रों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार नीतियों को आकार देने का अधिकार देता था। आपातकाल के दौरान शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने से (जून 1975 से मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि जब पूरे भारत में आपातकालीन शक्तियां लागू की गईं, जिससे नागरिक स्वतंत्रता में कटौती हुई) केंद्र सरकार को इस क्षेत्र पर अधिक नियंत्रण मिला।