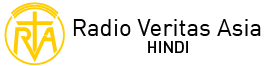हम सब बोलना कब भूल गए?

भारतीय राजनीति में "बेशर्म" शब्द का इस्तेमाल लगातार होता रहता है। लेकिन जब हाल ही में एक विपक्षी नेता ने पूछा कि क्या चुप्पी में 'च' का मतलब बेशर्मी है, तो यह बात दिल को छू गई। यह सवाल बहुत गहरा है क्योंकि यह उस भावना को बताता है जो हममें से कई लोग पब्लिक लाइफ को देखते हुए महसूस करते हैं — बड़ी-बड़ी स्पीच या वायरल गुस्से में नहीं, बल्कि उन बातों में जो कही नहीं जातीं, उन सवालों में जिनसे बचा जाता है, और उस गुस्से में जो कभी सामने नहीं आता।
सोचिए 5 जनवरी को क्या हुआ। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दो छात्र एक्टिविस्ट, उमर खालिद और शरजील इमाम को ज़मानत देने से मना कर दिया, जिससे वे आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत बिना मुक़दमे के सालों तक जेल में रहे। दोनों को 2020 के दिल्ली दंगों के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक विवादित नागरिकता कानून के विरोध प्रदर्शनों के बीच दर्जनों लोग मारे गए थे। अधिकारियों ने उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया, जबकि हिंसा में शामिल दूसरे लोग आज़ाद घूम रहे हैं।
कानूनी विशेषज्ञों ने जजों पर सरकारी दबाव की ओर इशारा किया। मुझे फैसले से ज़्यादा इस बात पर हैरानी हुई कि यह कितनी खामोशी से हुआ। कुछ विरोध प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर थोड़ा गुस्सा, फिर चुप्पी। मुख्य विपक्ष ने मुश्किल से ही कोई प्रतिक्रिया दी। जब अन्याय रोज़ की बात हो जाए और सत्ता में बैठे लोग चुप रहें, तो यह हमें क्या बताता है?
यह पैटर्न हर जगह दोहराया जाता है। जब अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप किया, तो भारत आश्चर्यजनक रूप से चुप रहा। जब वाशिंगटन ने रूस या ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी — जिससे भारत के तेल आयात पर बुरा असर पड़ा — तो प्रतिक्रिया धीमी चिंता और चुपचाप निवेश कम करने की थी। भारत को कभी इस बात पर गर्व था कि वह महाशक्तियों के सामने नहीं झुकता। वह आवाज़ अब खो गई लगती है, और यह चुप्पी रणनीति से ज़्यादा आत्मसमर्पण जैसी लगती है।
यह चुप्पी उन संस्थानों तक भी फैली हुई है जो ऐतिहासिक रूप से नैतिक गवाही के लिए जाने जाते हैं। जब 2021 में जेसुइट पादरी फादर स्टेन स्वामी की हिरासत में मौत हो गई, जिन्हें आदिवासी ज़मीन के अधिकारों की रक्षा करने के लिए आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत जेल में डाला गया था, तो चर्च की संस्थागत प्रतिक्रिया बहुत सोच-समझकर दी गई।
जब चर्चों पर हमले होते हैं या ईसाई संगठनों पर विदेशी फंडिंग की जांच होती है जिससे उनका काम रुक जाता है, तो आधिकारिक बयान टकराव से बचते हैं। व्यक्तिगत पादरी और नन अभी भी ज़मीनी स्तर पर बहादुरी से काम करते हैं, लेकिन संस्थागत आवाज़ हर शब्द को सोच-समझकर बोलती है ताकि उन्हें विदेशी एजेंट का लेबल न लगे या सरकार उनके स्कूलों पर कब्ज़ा न कर ले।
अदालतें ऐसे फैसले सुनाती हैं जिन्हें एक्टिविस्ट विनाशकारी कहते हैं, फिर भी बार एसोसिएशन चुप रहते हैं। जिन विश्वविद्यालयों में कभी बहस होती थी, अब वहां छात्र संगठित होने से डरते हैं। मीडिया सत्ता पर सवाल उठाने के बजाय उसे बढ़ावा देता है। हर चुप संस्था दूसरी संस्थाओं को मज़बूत करती है, जिससे एक ऐसा माहौल बनता है जहां बोलना तेज़ी से बेकार या खतरनाक लगता है। पूरे दक्षिण एशिया में युवा लोग बिल्कुल भी चुप नहीं रहे हैं। बांग्लादेश में छात्रों ने बड़े विरोध प्रदर्शनों के ज़रिए अपनी सरकार गिरा दी। श्रीलंका और नेपाल में प्रदर्शनों ने राजनीतिक बदलाव लाए। भारतीय युवाओं को क्या चीज़ अलग बनाती है? यहाँ निगरानी बहुत ज़्यादा है — इंटरनेट बंद करना, फ़ोन ट्रैक करना, और विरोध प्रदर्शनों में चेहरे की पहचान।
दांव भी ज़्यादा ऊंचे लगते हैं। भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले बांग्लादेशी छात्र को पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन एक भारतीय छात्र पर आतंकवाद के आरोप लग सकते हैं जो उसका पूरा भविष्य बर्बाद कर सकते हैं। भारत की मौजूदा स्थिति में एक घुटन भरी ध्रुवीकरण भी है, जहाँ किसी भी आलोचना को या तो हिंदू समर्थक या मुस्लिम समर्थक, राष्ट्र समर्थक या राष्ट्र विरोधी के रूप में देखा जाता है, और सिर्फ़ न्याय समर्थक होने की कोई जगह नहीं है।
इसमें एक क्रूर विरोधाभास भी जोड़ें: अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के विपरीत जो आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, कई मध्यम वर्गीय भारतीय युवाओं के पास बस इतना है — टेक में अच्छी नौकरियाँ, आरामदायक घर, विदेश में पढ़ाई के मौके — कि चुप रहना उन्हें समझदारी लगता है। जब आपके पास खोने के लिए कुछ हो तो सब कुछ जोखिम में क्यों डालना?
यह सोची-समझी चुप्पी, जो अज्ञानता से नहीं बल्कि फ़ायदे-नुकसान के विश्लेषण से पैदा हुई है, शायद सबसे खतरनाक तरह की चुप्पी है।
इस चुप्पी की कीमत इस बात से पता चलती है कि अब विवादास्पद कानून कितनी आसानी से पास हो जाते हैं। संघवाद या अल्पसंख्यक अधिकारों को कमज़ोर करने वाले उपाय आसानी से पास हो जाते हैं क्योंकि जनता का दबाव कमज़ोर है। सरकार यह जानती है। चुप्पी उन्हें कम जवाबदेही के साथ तेज़ी से आगे बढ़ने की जगह देती है।
मैं तमिलनाडु में पला-बढ़ा हूँ, जहाँ राजनीतिक बहस रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। वहाँ भी कुछ बदल गया है।
नेता अपने एजेंडे के हिसाब से सांस्कृतिक मुद्दों पर अपनी राय बदलते रहते हैं, जबकि व्यापक विपक्ष की चुप्पी से सत्ता नई दिल्ली में केंद्रित होती जा रही है। हमारी एक पुरानी तमिल कहावत है: हर जगह हमारी जगह है, हर कोई हमारा अपना है। जब दूसरे लोग दुख झेल रहे हों तो चुप रहना उस सिद्धांत के साथ धोखा है।
बेशक, चुप्पी अपने आप में शर्मनाक नहीं है। भारतीय दर्शन में यह जानना ज़रूरी है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। परेशानी तब शुरू होती है जब चुप्पी पसंद की जगह डिफ़ॉल्ट बन जाती है, जब यह सोच के बजाय डर से आती है, जब यह कमज़ोरों के बजाय ताकतवरों को बचाती है।