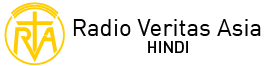भारत के श्रम सुधार कलीसिया की अंतरात्मा की परीक्षा ले रहे हैं

जब भारत ने 21 नवंबर को 29 औपनिवेशिक काल के श्रम कानूनों को चार आसान कोड में बदला, तो सरकारी मंत्रियों ने इसे ऐतिहासिक प्रगति बताया, और बिजनेस लीडर्स ने कम लालफीताशाही का जश्न मनाया। जब फैक्ट्री मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट्स को फिर से लिख रहे थे और गिग वर्कर्स नए फायदों को लेकर उलझन में थे, तो इस उथल-पुथल के बीच मैंने खुद से एक आसान सवाल पूछा: हम असल में यहां किसका भविष्य बना रहे हैं?
यह वादा लुभावना लगता है। गुजरात राज्य के सूरत में एक कपड़ा निर्माता को अब मजदूरी, सुरक्षा और सोशल सिक्योरिटी के लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन में नहीं उलझना पड़ता। फिक्स्ड-टर्म वर्कर्स को अब वे सुरक्षा मिलती हैं जो पहले सिर्फ परमानेंट कर्मचारियों के लिए थीं।
बेंगलुरु के अराजक ट्रैफिक में काम करने वाले डिलीवरी राइडर्स को आखिरकार हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन योजनाओं का फायदा मिलेगा, जिसमें प्लेटफॉर्म सोशल सिक्योरिटी के लिए टर्नओवर का दो प्रतिशत तक योगदान देंगे। ये बदलाव इस बात को मानते हैं कि आज भारत असल में कैसे काम करता है, जहां नौकरियां हमारे दादा-दादी की कल्पना से भी तेज़ी से बदल रही हैं।
फिर भी, मैं इन रिफॉर्म्स की जितनी गहराई से जांच करता हूं, उतना ही मुझे इस बात की चिंता होती है कि हम क्या खो रहे हैं।
कंपनियां अब सरकारी मंजूरी के बिना 300 कर्मचारियों तक को नौकरी से निकाल सकती हैं, जो पिछली सीमा से तीन गुना ज़्यादा है। बिजनेस ग्रुप इसे ज़रूरी लचीलापन कहते हैं। कर्मचारी इसे मनमानी बर्खास्तगी के खिलाफ अपनी एकमात्र ढाल का खत्म होना मानते हैं।
अब एक मान्यता प्राप्त यूनियन बनाने के लिए 51 प्रतिशत कर्मचारियों के समर्थन की ज़रूरत होगी, जिससे यह काम तब और मुश्किल हो गया है जब थके हुए कर्मचारी संगठन बनाने का जोखिम नहीं उठा सकते। सरकार इसे फालतू हड़तालों को रोकने के तौर पर पेश करती है। कर्मचारी इसे अपनी आवाज़ को दबाने के तौर पर अनुभव करते हैं, जब बोलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है।
घरेलू बजट को परेशान करने वाला गणित एक और समस्या दिखाता है। बेसिक सैलरी अब कुल मुआवजे का कम से कम आधा होनी चाहिए, जिससे प्रोविडेंट फंड में योगदान तो बढ़ेगा, लेकिन मासिक टेक-होम इनकम कम हो जाएगी।
हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो महीने में 50,000 रुपये (US$556.65) कमाती है, उसकी सैलरी से पांच हज़ार रुपये कम हो सकते हैं, यह वही पैसा था जिससे वह अपनी बेटी की ट्यूशन फीस देती थी या अपने बूढ़े माता-पिता के मेडिकल बिलों में मदद करती थी।
सरकार लंबे समय की सुरक्षा का वादा करती है, लेकिन आज की महंगाई से जूझ रहे परिवारों को अभी कैश चाहिए, न कि दूर के पेंशन लाभ जो शायद उन्हें कभी मिलें ही नहीं।
ये बदलाव सीधे चर्च के संस्थागत दिल पर चोट करते हैं। कैथोलिक डायोसीज़, धार्मिक मंडलियां और चैरिटेबल ट्रस्ट स्कूलों, अस्पतालों और सोशल सर्विस सेंटरों में लाखों लोगों को रोज़गार देते हैं।
दक्षिणी केरल राज्य का एक डायोसीज़ स्कूल अचानक अपरिचित डिजिटल पोर्टल्स से जूझ रहा है। पूर्वी झारखंड राज्य का एक जेसुइट सेंटर कम्युनिटी ऑर्गनाइज़र को काम पर रखने के बदले हुए नियमों से जूझ रहा है। अस्पताल चलाने वाले धार्मिक संगठनों को प्रोविडेंट फंड की नई कैलकुलेशन का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पहले से ही गरीबों की सेवा में लगे उनके बजट पर और दबाव पड़ रहा है।
यह कानून सेंट्रल इंडिया के ग्रामीण छत्तीसगढ़ में टीबी मरीजों का इलाज करने वाले मिशनरी अस्पताल को ठीक उसी तरह मानता है जैसे नेशनल कैपिटल नई दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम में गुरुग्राम (पहले गुड़गांव) में एक टेक कॉर्पोरेशन को, मकसद और संसाधनों में बुनियादी अंतर को नज़रअंदाज़ करते हुए।
जब डायोसीज़ बढ़े हुए पेरोल कटौती को पूरा करने और साथ ही मुफ्त मेडिकल कैंप चलाने में संघर्ष कर रहे हैं, तो ये सुधार भारत के सामाजिक ताने-बाने में चर्च की खास भूमिका के प्रति उनकी उदासीनता को दिखाते हैं।
इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि ये बदलाव चर्च के अपने कर्मचारियों को प्रभावित करते हैं, जिनमें से कई उन्हीं समुदायों से हैं जिनकी हम सेवा करते हैं। सेमिनरी में खाना बनाने वाला, चर्च के मैदान की देखभाल करने वाला माली, और पैरिश रिकॉर्ड संभालने वाला ऑफिस स्टाफ अब हर जगह के कर्मचारियों जैसी ही कमजोरियों का सामना कर रहा है।
चर्च की प्रतिक्रिया सिर्फ संस्थागत आत्म-रक्षा नहीं हो सकती। हमारी विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि हम जिस न्याय का उपदेश देते हैं, उसे अमल में लाते हैं या नहीं। इसका मतलब है कि सबसे पहले यह सुनिश्चित करना कि हर चर्च संस्थान इन नए नियमों के तहत एक मॉडल एम्प्लॉयर बने, न्यूनतम मानकों को बेमन से पूरा न करे, बल्कि जानबूझकर उनसे आगे बढ़े।
जब कोई पैरिश यह दिखाता है कि उसके कर्मचारियों को उचित वेतन, सम्मानजनक व्यवहार और कानूनी ज़रूरतों से परे सुरक्षा मिलती है, तो उसे दूसरों के लिए आवाज़ उठाने का नैतिक अधिकार मिलता है।
कैथोलिक सामाजिक शिक्षा की मांग है कि हम इन सुधारों की चपेट में आए कर्मचारियों के लिए खुलकर आवाज़ उठाएं। बिशप को पोप के आदेशों के नज़रिए से इन नियमों का विश्लेषण करना चाहिए, यह बताते हुए कि वे कहाँ मानवीय गरिमा को आगे बढ़ाते हैं और कहाँ वे श्रम को एक वस्तु बनाते हैं।
पैरिश पादरियों को रविवार के उपदेशों को अमूर्त धर्मशास्त्र से व्यावहारिक मार्गदर्शन में बदलना चाहिए। जब किसी पैरिश के सदस्य की नौकरी इसलिए चली जाती है क्योंकि छंटनी की सीमा तीन गुना हो गई है, तो चर्च भगवान की योजना के बारे में सामान्य बातें कहकर जवाब नहीं दे सकता। हमें उसे उसके कानूनी अधिकारों को समझने में मदद करनी चाहिए, उसे संसाधनों से जोड़ना चाहिए, और चर्च संस्थानों सहित नियोक्ताओं पर दबाव डालना चाहिए कि वे नौकरी से निकालने को आखिरी उपाय के तौर पर देखें।