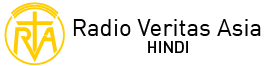भारत के धर्मांतरण विरोधी कानून और विवेक का संकट

सिलीगुड़ी, 19 सितंबर, 2025 — "मैंने धर्म के लिए नहीं, प्रेम के लिए विवाह किया था। लेकिन अब, मेरे साथ एक अपराधी जैसा व्यवहार किया जा रहा है।"
ये शब्द उत्तर प्रदेश की 24 वर्षीय आयशा (बदला हुआ नाम) के थे, जिनके अंतरधार्मिक विवाह ने राज्य के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत पुलिस की जाँच का कारण बना। उनके पति, जो एक ईसाई हैं, पर "प्रलोभन" का आरोप लगाया गया था - एक ऐसा शब्द जो इतना लचीला है कि इसमें स्नेह, शिक्षा, यहाँ तक कि सहभोज भी शामिल हो सकता है।
भारत भर में, आयशा जैसी कहानियाँ बढ़ रही हैं। प्रार्थना सभाओं में बाधा डाली जा रही है। पादरियों को हिरासत में लिया जा रहा है। धर्मांतरित लोगों से पूछताछ की जा रही है। 1968 में मध्य प्रदेश में ज़बरदस्ती रोकने के लिए जो कानून बनाया गया था, वह अब संदेह के एक ऐसे शासन में बदल गया है, जहाँ आस्था का डर है, और आज़ादी नौकरशाही के ज़रिए छनकर आती है।
"संविधान मुझे अपना धर्म चुनने का अधिकार देता है। मुझे सरकार से अनुमति क्यों मांगनी चाहिए?" मध्य प्रदेश के एक दलित युवक रमेश (बदला हुआ नाम) पूछते हैं, जिन्होंने वर्षों के जातिगत भेदभाव के बाद ईसाई धर्म अपना लिया। उनके बपतिस्मा की सूचना उनके एक पड़ोसी ने दी, जिसके बाद पुलिस ने जाँच शुरू कर दी।
ये कोई अलग-थलग घटनाएँ नहीं हैं। ये एक गहरी अस्वस्थता को दर्शाती हैं—धार्मिक बहुलता के प्रति बढ़ती बेचैनी और व्यक्तिगत विवेक के लिए सिकुड़ती जगह।
जब राज्य विवेक का रक्षक बन जाता है
ओडिशा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, हरियाणा और हाल ही में राजस्थान सहित एक दर्जन राज्यों ने धर्मांतरण को नियंत्रित करने वाले कानून बनाए हैं या उनमें संशोधन किया है।
महाराष्ट्र ने भी इसी तरह का कानून प्रस्तावित किया है। हालाँकि इन्हें "धर्म स्वतंत्रता अधिनियम" के रूप में तैयार किया गया है, लेकिन इन कानूनों में अक्सर अधिकारियों को पूर्व सूचना देने, तीसरे पक्ष की शिकायत की अनुमति देने और कठोर दंड लगाने की आवश्यकता होती है, खासकर विवाह से जुड़े धर्मांतरण के लिए।
हालाँकि भाषा अलग-अलग है, लेकिन इरादा स्पष्ट है: राज्य अक्सर बहुसंख्यकवादी राजनीति के दबाव में, व्यक्तिगत आस्था के मामलों में खुद को शामिल कर रहा है। इसका परिणाम धार्मिक स्वतंत्रता पर, खासकर ईसाइयों, मुसलमानों, दलितों और अंतरधार्मिक जोड़ों पर, एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
जब आस्था की परीक्षा ली जाती है
भारत का संविधान किसी व्यक्ति को अपनी आस्था को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है। लेकिन धर्मांतरण-विरोधी कानून इस वादे को उलट देते हैं। ये धर्मांतरित व्यक्ति पर सबूत का भार डालते हैं, आध्यात्मिक यात्राओं को अपराध मानते हैं और अंतरात्मा को निषिद्ध मानते हैं।
कानूनी विद्वानों का तर्क है कि ये कानून इन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं: अनुच्छेद 25: अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21: व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता का संरक्षण। अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता।
सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को एक साथ मिला दिया है। हाल की सुनवाई में, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यों से यह स्पष्ट करने को कहा कि वे "जबरदस्ती" और "प्रलोभन" को कैसे परिभाषित करते हैं, - ये शब्द इतने अस्पष्ट हैं कि इनसे करुणा, शिक्षा या प्रेम का अपराधीकरण होने का खतरा है।
जब अदालत विचार-विमर्श कर रही है, तो राष्ट्र देख रहा है। क्या वह संविधान की भावना को कायम रखेगी या राज्य को आस्था पर हुक्म चलाने देगी?
सच्ची आस्था स्वतंत्रता में पनपती है, भय में नहीं।
यह क्षण कानूनी स्पष्टता से कहीं अधिक की मांग करता है। इसके लिए नैतिक साहस की आवश्यकता है। सुसमाचार हमें सिखाता है कि विश्वास प्रेम का प्रतिउत्तर है, भय का प्रतिउत्तर नहीं। यीशु ने कभी दबाव नहीं डाला; उन्होंने आमंत्रित किया। उन्होंने कभी निगरानी नहीं की; उन्होंने चंगा किया। उन्होंने साधकों को कभी दंडित नहीं किया; उन्होंने उनका स्वागत किया।
उनके मंत्रालय पर विचार करें: दो जिज्ञासु शिष्यों से, उन्होंने कहा, "आओ और देखो" (यूहन्ना 1:39) — कोई दबाव नहीं, केवल निमंत्रण। थके हुए लोगों को, उन्होंने विश्राम दिया: "मेरे पास आओ।" (मत्ती 11:28)। प्रकाशितवाक्य में, वह द्वार पर खड़े होकर दस्तक देते हैं — भीतर घुसकर नहीं (प्रकाशितवाक्य 3:20)।
उन्होंने रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री को स्थिर किया (मरकुस 5), अंधे व्यक्ति को स्वस्थ किया (यूहन्ना 9), और दस कोढ़ियों को चंगा किया—बिना धन्यवाद मांगे (लूका 17)। उन्होंने पापी स्त्री का स्वागत किया (लूका 7), सामरी स्त्री के सामने स्वयं को प्रकट किया (यूहन्ना 4), और घृणित चुंगी लेने वाले जक्कई को गले लगाया (लूका 19)।
ये सिर्फ़ बाइबिल के क्षण नहीं हैं - ये नैतिक आदर्श हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा विश्वास स्वतंत्रता में पनपता है, भय में नहीं।
अंतरात्मा की गरिमा की रक्षा
ऐसे कानूनों के सामने जो इरादे को गलत समझते हैं और दोषसिद्धि को आपराधिक ठहराते हैं, चर्च को स्पष्टता, साहस और करुणा के साथ जवाब देना चाहिए। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि धर्मांतरण कोई लेन-देन नहीं है - यह एक परिवर्तन है। यह चिंतन, साक्षात्कार और अनुग्रह का फल है।
जब व्यक्ति मसीह का अनुसरण करने का चुनाव करते हैं, तो वे अपनी गहनतम स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं: सत्य के प्रति अपनी समझ के अनुसार प्रतिक्रिया देने की स्वतंत्रता। इसकी रक्षा एक पवित्र अधिकार के रूप में की जानी चाहिए, न कि एक संदिग्ध कृत्य के रूप में।
पोप बेनेडिक्ट सोलहवें ने कहा था, "विश्वास थोपा नहीं जाता - यह प्रस्तावित होता है।" चर्च को हर मंच पर इसे दोहराना चाहिए।
अपने विश्वास को चुनने का अधिकार एक ईसाई मुद्दा नहीं है - यह एक मानवीय मुद्दा है। चर्च को चाहिए: अदालतों, कक्षाओं और धर्मोपदेशों में विवेक की रक्षा करें। जांच के दायरे में आने वालों को पादरी देखभाल और कानूनी सहायता प्रदान करें।
अंतर-धार्मिक एकजुटता को बढ़ावा दें, तथा राष्ट्र को याद दिलाएं कि उसकी ताकत एकरूपता में नहीं, बल्कि विविधता में निहित है।